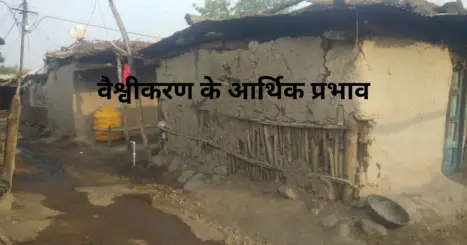आदिवासी समुदायों की अर्थव्यवस्था प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित है। (ऊपरी तौर पर अनायास प्राप्त होने वाले साधन और वनोपज) इस व्यवस्था में साधारण-सी कृषि पद्धतियाँ प्रचलित होती हैं, यह व्यक्ति प्रदान नहीं बल्कि समूह प्रधान है लेकिन आज इस अर्थव्यवस्था को Vaishvikaran ke Aarthik prabhav ने तहस-नहस कर चुका है।
आदिवासी अर्थव्यवस्था का संक्षिप्त परिचय:
आदिवासी समाज मध्यवर्ती वस्तु के स्थान पर प्राथमिक व अंतिम उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन करता है। जिसके फलस्वरुप उनकी आय में चक्रीय वृद्धि नहीं हो पाती है। आदिवासी अर्थव्यवस्था के संदर्भ में रामदयाल मुंडा लिखते हैं कि “संसार के सभी आदिवासी क्षेत्र की तरह झारखंडी अर्थव्यवस्था भी सामुदायिक, सामूहिकता पर आधारित है, जिसके अनुसार हवा की तरह जमीन, जंगल और जल व्यक्तिगत संपत्ति न होकर सामुदायिक संसाधन हैं” आदिवासी अस्तित्व और झारखंडी अस्मिता के सवाल, पृष्ठ-33, अर्थात इस व्यवस्था में प्राकृतिक संसाधनों का समान प्रयोग के सिद्धांत की प्रधानता है। इतना ही नहीं आदिवासी समुदायों में प्राकृतिक उत्पादन के संग्रह के पश्चात समान वितरण का सिद्धांत भी प्रचलित है। आदिवासी समुदायों की अर्थव्यवस्था में सहभागिता की प्रवृत्ति प्रमुख है किंतु आधुनिक पूँजीवादी समाज की अर्थव्यवस्था संग्रह प्रधान है। इसके संदर्भ में रामदयाल मुंडा लिखते हैं कि “अर्थव्यवस्था के सामुदायिक होने का यह भी मतलब है कि वह सहभागिता पर आधारित है, जबकि आधुनिक अर्थव्यवस्था एकाधिकार/संचय पर जोर देती है” आदिवासी अस्तित्व और झारखंडी अस्मिता के सवाल, पृष्ठ-33, यदि हम वैश्वीकरण कि पूँजीवादी अर्थव्यवस्था और आदिवासी अर्थव्यवस्था की आपसी टकराव जब देखते हैं, तब आदिवासी अर्थव्यवस्था की पराजय हो जाती है, जिसके फलस्वरूप हाल में हुई आर्थिक जनगणना के आंकड़े बताते हैं कि “भारत में अन्य समुदायों की तुलना में गरीबी रेखा के नीचे जिंदगी बसर करने वालों में जनजातियों की जनसंख्या सबसे अधिक है।” आदिवासी भाषा और शिक्षा, पृष्ठ-87, पूँजीवादी अर्थव्यवस्था का सर्प विश्व के समस्त संसाधनों पर एक छत्र अधिकार का जाल बिछाकर उस जाल पर बैठा है, जो सीमांत समुदायों की ओर अपना फन बढ़ाता ही जा रहा है। यह व्यवस्था सब कुछ छीन लेना चाहती है, फिर वह संसाधन हो, परंपरा हो, संस्कृति हो, आत्मसम्मान हो, आत्मगौरव हो या स्वाभिमान हो। वह वर्तमान सभ्यता को अपने अनुकूल चलाना चाहती है, जिसमें अनेक समुदायों का अस्तित्व ही मिट जाने का संकट मंडरा रहा है।
आप यहाँ वैश्वीकरण और आदिवासी अस्मिता का प्रश्न पर आलेख पढ़ सकते हैं।
पूँजीवाद का परिचय:
वैश्वीकरण का शाब्दिक अर्थ “स्थानीय या क्षेत्रीय वस्तुओं या घटनाओं के विश्व स्तर पर रूपांतरण की प्रक्रिया है।” विकिपीडिया पूँजी के चरित्र को परिभाषित करते हुए हरिराम मीणा लिखते हैं कि “पूँजी के चरित्र की दो प्रमुख विशेषताएँ हैं। यह एक व्यक्तिवादी, जहाँ व्यक्ति केंद्र में होता है, मनुष्य नहीं। इसलिए अन्य हितों की अनदेखी होती है और निजी स्वार्थ सर्वोपरि। दूसरा निजीकरण इसका केंद्रीय तत्व होता है, जिसमें लोक प्रशासन अर्थात राज्य की भूमिका अत्यंत सीमित होती है। व्यक्ति घराना, कंपनी या कार्पोरेशन अपना अनियंत्रित विस्तार करता है। अतः बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ अस्तित्व में आती हैं, जो प्रत्यक्ष रूप से निजीकृत, आर्थिक साम्राज्यवाद का ही दूसरा रूप है। परोक्ष रूप से यह स्थिति राजनीति, संस्कृत, समाज एवं जीवन के अन्य पक्षों को भी प्रभावित करती है। राष्ट्र के स्तर पर पूँजीवादी व्यवस्था क्रूर साम्राज्यवाद को जन्म देती है।” प्रगतिशील वसुधा , पृष्ठ 85, पूँजी के चरित्र को परिभाषित करते हुए आदिवासी विचारक हरिराम मीणा ने उन तमाम सवालों एवं चुनौतियों को स्पष्ट कर दिया है, जिन सवालों एवं चुनौतियों से आज का आदिवासी समाज जूझ रहा है।
पूँजीवादी अर्थव्यवस्था की ये प्रवृत्तियाँ आज के युग का सत्य है और यह सत्य अपने अनियंत्रित विस्तार को बढ़ाने की प्रक्रिया में विश्व के तमाम संसाधन बहुल क्षेत्रों एवं समुदायों की विश्वदृष्टि में मनमाना हस्तक्षेप कर रहा है। यह हस्तक्षेप केवल आर्थिक स्थिति को ही नहीं बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक, जीवन मूल्य तथा अस्तित्व को भी नकारात्मक रूप में प्रभावित कर रहा है।
आज के दौर में आदिवासी समाज आर्थिक दृष्टि से बहुत पीछे रह गया है। जिसके कई कारण भी हैं। इन कारणों को हम दो श्रेणियों में विभक्त कर सकते हैं। एक आंतरिक कारण है और दूसरा बाह्य कारण।
आंतरिक कारण की यदि हम व्याख्या करें, तो स्पष्ट रूप में कहना होगा कि भारतीय आदिवासी समाज अन्य समाज के आर्थिक, राजनीतिक सरोकारों से अपने समाज में प्रचलित आर्थिक, राजनीतिक सरोकारों के साथ सामंजस्य बिठा नहीं पाया है। वह परंपरागत जीवन मूल्य तथा आर्थिक सरोकारों के साथ प्रकृति के गोद में पड़ा रहा, जहाँ विकास की संभावनाएँ अत्यंत न्यून थीं।
यदि हम बाह्य कारणों की पड़ताल करें, तो दृष्टिगोचर होता है, कि आधुनिक पूँजीवाद ने संसाधनों की खोज में इन समाज व्यवस्थाओं में हस्तक्षेप किया और आदिवासी मानदंडों को प्रभावित किया तथा अपने वैश्विक हथकंडों द्वारा प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। इस प्रक्रिया ने आदिवासी समाज को आर्थिक विकास की धारा से और भी अलग-थलग कर दिया।
वर्तमान स्थिति यह है, कि पूँजीवाद आदिवासी समुदायों के अस्तित्व को मिटाने का भरसक प्रयास कर रहा है।

आदिवासी समुदायों की अर्थव्यवस्था पर वैश्वीकरण और पूँजीवाद का प्रभाव: vaishvikaran ke Aarthik prabhav
आदिवासी समाज सीधा-साधा जीवन व्यतीत करता है, उनकी अर्थव्यवस्था संग्रह प्रधान नहीं बल्कि निर्वाह प्रधान है। इसका प्रमुख कारण यह है, कि वह अपने साथ-साथ प्रकृति के जीव-जन्तु एवं प्राणियों का भी ध्यान रखता है। यदि वनों में किसी पेड़ पर पके हुए फल हैं, तो वह वृक्ष से नीचे गिरे हुए फल को लेगा अथवा उस वृक्ष से उतने ही फल लेगा, जितने फलों से उसका उसी समय पेट भर सके। वही वैश्वीकरण के मुख्य धारा का समाज उस वृक्ष से पके हुए सारे फलों को ले लेगा और कच्चे फलों को भी तोड़ कर अपने घर में पकने हेतु व्यवस्था करेगा। अपना पेट भर जाने के बाद वह बाज़ार में उन फलों को विक्रय हेतु प्रस्तुत करेगा, यहीं नहीं वह उस वृक्ष के चारों ओर चिन्हित कर अपना अधिकार भी सिद्ध करने लगेगा। यहीं अन्तर है, वैश्वीकरण की अर्थव्यवस्था और आदिवासी अर्थव्यवस्था के बीच। एक कविता में उनकी प्रवृति का चित्रण हुआ है।
‘‘प्रकृति संग प्रेम मय धागा,
अल्प संतुष्टि, संग्रह प्रवृत्ति त्यागा
जिसका मिल रहा प्रतिफल
नयन जल, जल रहा अनल।” राठोड पुंडलिक, जंगल के अंधियारे से…अनंग प्रकाशन दिल्ली, 2019, पृष्ठ-34
आदिवासी समाज संग्रह नहीं करता अल्प संसाधनों में ही वह संतुष्ट रहता है किन्तु आज वैश्वीकरण ने उनके जीवन मूल्य एवं उनकी मौलिक प्रवृति को ही समाप्त कर दिया है। कारण वैश्वीकरण की संस्कृति व्यावसायिक संस्कृति है। वह हर चीज यहाँ तक कि संबंधों को भी वस्तु की दृष्टि से देखता है। इसपर ब्रज कुमार पाण्डेय लिखते हैं कि ‘‘व्यावसायिक संस्कृति समाज की हर चीज को बिकाऊ, बनाती है, वह समाज की जरूरत को नहीं, मुनाफे की जरूरत को व्यक्त करती है। बाजार तंत्र की विशेषताएँ यह हैं कि उसे खरीद-बिक्री करनेवालों की जरूरत है, सबसे जादा खरीदनेवालों का महत्व है, जो खरीदने की क्षमता नहीं रखता ……. वह आदमी बाजार तंत्र के लिए एकदम बेकार है।” अभय कुमार दुबे, भारत का भूमंडलीकरण – ग्रथ अकादमी दिल्ली, पृष्ठ-94
आज का आदिवासी समाज विस्थापन से पीड़ित है, उनके रोजगार छीन लिए गए हैं, उनकी भूमि का अधिग्रहण हो चूका है और वे अपने जीवन यापन हेतु दर-दर भटक रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सरकार ने उनके पुनर्स्थापन की व्यवस्था नहीं की आवश्य की है किन्तु वे सारी व्यवस्थाएँ कागज़ों एवं फाइलों के हवाले हो गई। वैश्वीकरण की मानसिकता भारत के लोगों को ‘शायनिंग इडिया’ का स्वप्न दिखाती है। इस स्वप्न के पीछे बहुत कुछ होता है, जो साधारण जनता समझ नहीं पाती। शायनिंग इंडिया में लोगों की स्थिति देखें-
‘‘गरीब किसान और मजदूर
दलित-आदिवासी है, मजबूर
भूमंडलीकरण के नाम पर
हो गए बेचारे चकनाचूर।” भगवान गव्हाडे, आदिवासी मोर्चा, वाणी प्रकाशन नयी दिल्ली, 2014, पृष्ठ – 37
चकनाचुर होने के पीछे प्रमुख कारण पूँजीपतियों की घुसपैठ तथा आदिवासी निर्वाह प्रधान अर्थव्यवस्था का अन्त होना है।
अब यह बात स्पष्ट होती जा रही है कि वैश्वीकरण के समस्त फायदे समाज के भद्र वर्ग को मिलते रहे हैं, जिनके अधिकार में प्रमुख शक्तियाँ तथा साधन-संसाधन रहते आए हैं। निज-धन-ज्ञान-धर्म की शक्तियाँ, पूँजी, बाजार, तकनीकी, उच्च शिक्षा तथा अन्य सुविधाएँ उन्हीं के पास मौजूद हैं किन्तु दूसरी और आम आदमी गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी, अच्छी शिक्षा का अभाव, स्वास्थ्य की समस्याएँ, पेयजल आपूर्ति का संकट तथा अन्य आधारभूत सुविधाओं से जूझ रहा है।
‘‘न बचा कंद और न बचा मूल
कब के हो चुके सब गायब
भूख के मारे सट गया है पेट
पीठ से” वाहरू सोनवणे, पहाड हिलने लगा है, शिल्पायन पब्लिकेशन दिल्ली, 2009, पृ-29
यह स्थिति इसलिए उत्पन्न हुयी है कि सरकारे बहुराष्ट्रीय कम्पनियों से बड़े-बड़े करार करके इनके जल, जंगल, जमीन पूँजीपतियों को सौप दी है और पूँजीपति वहाँ के संसाधनो को लूटने हेतु आदिवासियों को विस्थापित करते हैं। ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि आदिवासियों का जीवन नर्क के समान हो गया है। उसका अस्तित्व ही खतरे में है, तब आदिवासी सोचने लगता है कि-
‘‘यहाँ रहकर क्या करें?
यहाँ हमें न सहारा है,
न पेट के लिए चारा,
न काम है न धंधा,
काम मांगने गया तो
किया लाठी से वार,
हमारा विश्वास हो गया घायल
दर्द अभी भी ताजा ही था” वाहरू सोनवणे, पहाड हिलने लगा है, शिल्पायन पब्लिकेशन दिल्ली, 2009, पृ-28
ऐसी स्थिति में आदिवासी अपने मूल क्षेत्र से पलायन करने लगता है। दर-दर भटकने लगता है तथा किसी शहर के कोने में झुग्गी झोपडियाँ बनाकर कुछ काम धंधा करने लगता है। शहरों में भी उनके श्रम का बहुत शोषण होता है।
शहरों में भी पूँजीवाद या वैश्वीकरण कहाँ उन्हें छोड़ेगा जब तक वह अपने प्राण न दे, तब तक शहरी क्षेत्रों में उनकी बस्तियो को उजाड़ने के अनेक षड्यंत्र षड़यन्त्र होने लगते हैं। वाहरू सोनवने की एक कविता देखे-
‘‘झोपड़ियों की बस्ती उन्हें
लगती है कचरे का गड्डा
और गरीबों का आसरा
बीमारी फैलाने का केन्द्र,
हमारे बच्चे लगते हैं
राह का रोडा,
तेजी से निकाल एक और आदेष
उखड़ती चली गई एक-एक झोपड़ी,
बुझ गई झोपड़ी की लालटेन
कदम कदम पर पसरा अंधेरा,
बाल-बच्चों के आसू रोकने के लिए
नहीं बचा आंगन,
अब तुम ही बताओं
कौन है हमारा …… इस धरती पर?
कोऽऽई नहीं है।” वाहरू सोनवणे, पहाड हिलने लगा है, शिल्पायन पब्लिकेशन दिल्ली, 2009, पृ-28
देखिए वैश्वीकरण ने सर्वप्रथम जंगलों में उनके संसाधनों पर कब्जा जमाया फलत: आदिवासी समुदाय विस्थापित हुए। आदिवासी अर्थव्यवस्था को समाप्त कर दिया, फिर उनकी भूमि का अधिग्रण किया। अतः वे विस्थापित हो गए और भटकते-भटकते शहरों में झुग्गी झोपड़ियों में रहने लगे और वहाँ भी उनके साथ यह व्यवहार हुआ अब विचारणीय मुद्दा है कि वैश्वीकरण क्या करने पर आमादा है। यह किस प्रकार का विकास है तथा इन लोगों के मानवाधिकार कहाँ गए। मानवाधिकार संरक्षण करनेवाली संस्थाएँ कहाँ सो गई। मानवाधिकार आयोग किस गहरी नींद में खर्राटे ले रहा है।
कहना न होगा कि वैश्वीकरण की अवधारणा वास्तव में जन साधारण के लिए है ही नहीं। यह कुछ चंद लोगों के हितों के लिए है। इस प्रक्रिया में प्राकृतिक संसाधनों की लुट तथा राष्ट्रीय संसाधनों का उपयोग राष्ट्र विकास में नहीं बल्कि किसी अन्यों के हितो में हो रहा है। इसके परिणाम स्वरूप आदिवासी अपना अस्तित्व खो रहा है।
आर्थिक भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। राजनेताओं से लेकर बिचौलियों तक सभी इसमें लिप्त हैं। आर्थिक मंदी के नाम पर आम आदमी के हितों की परवाह किए बिना औद्योगिक घरानों को अत्यधिक सुविधाएँ देने के लिए सरकारे मजबूर होती हैं। यदि वैश्वीकरण प्रक्रिया इतनी अच्छी है, तो बार-बार आर्थिक मंदी क्यो आ जाती है? इसी क्रम में जनता के धन का दुरूपयोग होने लगता है।
जनसेवा एवं सुविधाओं के नाम पर महत्वपूर्ण सार्वजनिक क्षेत्रों का निजीकरण होने लगता है। जिनमें शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रों में गुणवत्ता की बहानेबाजी से निजी लाभ को सर्वोपरी रखा जाता है। इनमें आम आदमी को अथवा जरूरतमंद लोगों को कोई सुविधाएँ नहीं मिलती हैं। ये सुविधाएँ केवल समर्थ लोग तक ही सीमित रह जाती हैं।
भूमंडलीकरण की प्रक्रिया में आम आदमी की सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि उसकी पहुँच राष्ट्रस्तरीय सरकारी व निजी प्रबंधन तक नहीं हो पाती। इस सीढ़ी युक्त व्यवस्था से आदिवासी समाज भी जूझ रहा है। आदिवासी समाज की पहुँच मीड़िया तथा जनसंचार माध्यमों तक भी नहीं होती है।
वैश्वीकरण का बाजारवाद अपने स्वभाव के अनुरूप आम आदमी तथा आदिवासी समुदाय तक न चाहते हुए भी पहुँच जाता है किन्तु आवश्यक मूलभूत चीज़े उचित दामों पर नहीं मिल पाती। उपभोग की वस्तुएँ राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्ध होती हैं, फिर भी वे आदिवासी समाज से दूर रहती हैं। जीवनयापन के जो तरीके आदिवासियों के पास परम्परागत रूप से विद्यमान थे, वे उनके हाथ से धीरे-धीरे खिसक जाते हैं । जैसे अनायास प्राप्त वनोपज, टोकरा बनाने की विधि, कुटीर उद्योग, छोटे उद्योग अर्थात वैश्वीकरण में पूँजी एवं बाजार हावी होता है, जिस पर एक चालाक वर्ग का अधिपत्य होता है और आम आदमी तथा आदिवासी धीरे-धीरे हाशिए पर चला जाता है।
अतः यह समय गभीर रूप से सोचने समझने का है तथा विचार करने का है कि ऐसा क्यो और कैसे हो रहा है। इन समस्याओं का सामना करने हेतु किन-किन कदमों की आवश्यकता है। इस पर आज विचार करने के आवश्यकता है।
आप यहाँ आदिवासी समाज पर वैश्वीकरण के सामाजिक प्रभाव पढ़ सकते हैं।
निष्कर्ष:
वैश्वीकरण का वास्तविक रूप पूँजीवाद, वैश्विक संसाधनों की खोज में आदिवासी क्षेत्रों में पहुँचकर वहाँ के संसाधनों पर अपना कब्जा जमा लिया और वहाँ के आदिवासी समुदायों की हजारों वर्ष पुरानी अर्थव्यवस्था और जीवन पद्धतियों को समाप्त कर दिया है। आदिवासी अर्थव्यवस्था को समाप्त कर दिया है। फलत: आदिवासी समुदाय अपनी जीविका चलाने हेतु विस्थापित हो रहें हैं और शहरों की ओर पलायन कर रहें हैं। शहरों में भी वे विभिन्न तरीकों से शोषित हो रहें हैं।